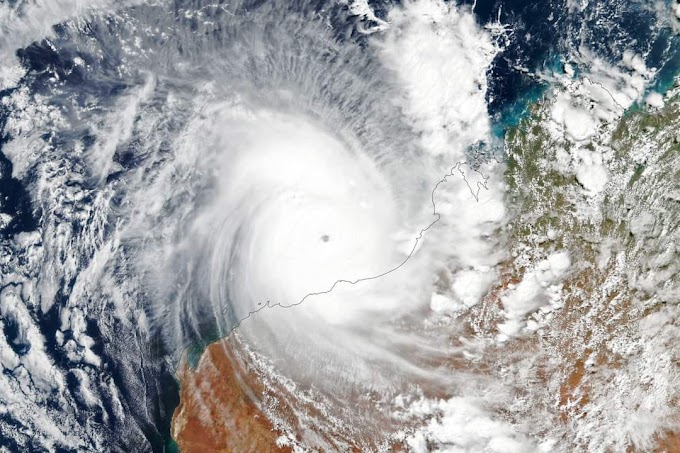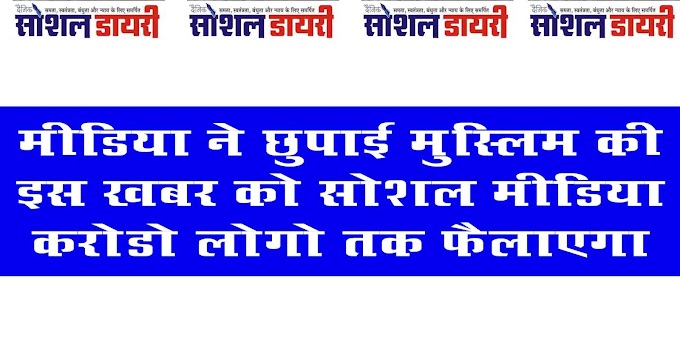सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने 26 सितंबर, 2016 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को लिखा ‘‘आपको तो यह पता ही होगा कि अखलाक नामक एक व्यक्ति को दादरी में कथित गौरक्षकों ने पीट-पीटकर मार डाला। इस भयावह अपराध को अंजाम देने वालों को सज़ा देने की बजाए, पुलिस और स्थानीय जज, अखलाक के परिवार के खिलाफ ही कार्यवाही कर रहे हैं...क्या पुलिस पागल हो गई है?’’
चांद खान उर्फ शान खान को अक्षरधाम मंदिर पर आतंकी हमले के मामले में सन 2002 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे 11 वर्ष जेल में बिताने के बाद, बिना किसी मुआवजे के रिहा कर दिया गया क्योंकि एक अदालत ने उसे बरी कर दिया। परंतु अब उसे गौहत्या के एक मामले में मुजरिम बना दिया गया है। मुफ्ती अब्दुल कय्यूम अब्दुल हुसैन की एक पुस्तक है, जिसका शीर्षक है ‘‘इलेविन इयर्स बिहाइन्ड द बार्स-आई एम ए मुफ्ती, नॉट ए टेरोरिस्ट’’ (सींखचों के पीछे ग्यारह साल-मैं एक मुफ्ती हूं, मैं आतंकवादी नहीं हूं)। यह पुस्तक मुफ्ती साहब के आतंकी हिंसा में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी, उनको शारीरिक यंत्रणाएं दिए जाने और उसके बाद, इतने लंबे अरसे तक जेल में रखे जाने की करूण गाथा कहती है। आमिर खान नाम के एक मुस्लिम लड़के को आतंकियों का साथ देने के आरोप में जब गिरफ्तार किया गया था, तब वह मेट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। चैदह साल जेल में काटने के बाद जब वह रिहा हुआ, तब तक उसके पिता गुज़र चुके थे और उसकी मां गंभीर रूप से बीमार थीं। उनकी पुस्तक ‘‘फ्रेम्ड एज़ ए टेरेरिस्ट’’ (आतंकी बताकर फंसाया गया) को पढ़ने से यह अंदाज़ा होता है कि हमारी व्यवस्था एक निर्दोष व्यक्ति के प्रति कितनी क्रूर हो सकती है।
ये तो कुछ उदाहरण मात्र हैं। ऐसे मुसलमान युवकों की एक लंबी सूची है जिन्हें आतंकवाद से संबंधित आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी जिंदगी थम गई और उनके करियर व परिवार तबाह हो गए। हाजी उमरजी को गोधरा ट्रेन आगजनी मामले का मास्टरमाइंड होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। कई साल जेल में बिताने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सुबूत नहीं मिला। मक्का मस्जिद (हैदराबाद), मालेगांव, समझौता एक्सप्रेस और अजमेर धमाकों के मामलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार किया गया और बाद में कोई विश्वसनीय सुबूत न पाए जाने पर रिहा कर दिया गया। इन सभी मामलों में पुलिस की जांच पूर्वाहग्रहपूर्ण और गलत थी। यह स्पष्ट है कि पुलिस, अल्पसंख्यकों के प्रति गहरे पूर्वाग्रह से ग्रस्त है। भारत में सांप्रदायिक हिंसा के अध्येता हमें बताते हैं कि ब्रिटिश काल में पुलिस की चाहे जो कमियां रही हों, सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में वह निष्पक्षता से काम करती थी। पुलिस के अल्पसंख्यकों के प्रति पूर्वाग्रहग्रस्त होने की शुरूआत, स्वाधीनता के बाद हुई और स्वतंत्र भारत में जबलपुर में 1961 में हुए पहले सांप्रदायिक दंगे के बाद से लेकर आज तक पुलिस का अल्पसंख्यक-विरोधी दृष्टिकोण और मानसिकता हम सबके सामने है। कई मौकों पर पुलिस के अलावा, राज्य तंत्र और राजनैतिक नेतृत्व ने भी निष्पक्षता नहीं दिखलाई। अधिकांश जांच आयोगों की रपटें, फिल्में और डोक्युमेंट्रियां इस तथ्य को रेखांकित करती हैं। सरकारी सेवाओं में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है और जो चंद मुसलमान उच्च पदों पर हैं, वे भी या तो धारा के साथ बहने लगते हैं या चुप्पी साध लेते हैं। अक्सर उन्हें ऐसे क्षेत्रों में पदस्थ किया जाता है जहां वे सांप्रदायिक हिंसा को रोकने या उसे करने वालों को सज़ा दिलवाने में सक्षम ही नहीं होते।
मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों पर श्रीकृष्ण न्यायिक जांच आयोग की रपट बताती है कि किस तरह पुलिस अधिकारियों ने दंगाईयों की हरकतों को नजरअंदाज किया और कई मामलों में उनका साथ दिया। दिल्ली में 1984 में हुई सिक्ख-विरोधी हिंसा और सन 2002 के गुजरात दंगों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। महाराष्ट्र के धुले में सन 2013 में पुलिस वाले स्वयं दंगाईयों की भूमिका में थे। हाशिमपुरा घटना पर अपनी पुस्तक में पूर्व पुलिस महानिदेशक वीएन राय ने बताया है कि किस प्रकार पुलिस ने एक ट्रक में मुस्लिम युवकों को भरा, उन्हें दूर ले जाकर गोलियों से भून दिया और फिर उनकी लाशें एक नहर में फेंक दीं। जो लोग जिंदा बच गए, वे इस भयावह घटनाक्रम को दुनिया के सामने लाए।
अमरीकी मीडिया ने 9/11/2001 को डब्ल्यूटीसी पर आतंकी हमले के बाद ‘इस्लामिक आतंकवाद’ शब्द गढ़ा। इस शब्द से ऐसा प्रतीत होता है मानो दुनिया में आतंकवाद के लिए केवल इस्लाम और मुसलमान ज़िम्मेदार हैं। मीडिया ने इस तथ्य को नज़रअंदाज़ कर दिया कि अल्कायदा को इतना शक्तिशाली बनाने वाला अमरीका ही था। तब से हालात और खराब हुए हैं। न केवल समाज बल्कि राज्यतंत्र भी मुसलमानों को आतंकी बतौर देखने लगा है। पूरे विश्व में इस्लाम के प्रति इस तरह का घृणा का वातावरण बनाने में मीडिया और निहित स्वार्थी तत्वों की भूमिका रही है।
जाहिर है, निर्दोष युवाओं और अन्यों को पुलिस और राज्य तंत्र की मनमानी से बचाए जाने की आवश्यकता है। पुलिस सुधारों के लिए कई आयोग गठित किए गए जिन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कई सुझाव दिए। परंतु अधिकांश सुझावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पुलिसकर्मियों को अल्पसंख्यकों के प्रति संवेदनशील बनाए जाने की ज़रूरत है। जिन अकादमियों और संस्थानों में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके पाठ्यक्रमों में पूर्वाग्रहों और टकसाली धारणाओं के पीछे के सच को उजागर करने वाली सामग्री शामिल की जानी चाहिए। पुलिसकर्मियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि भावनाओं में बहने की बजाए उन्हें संविधान और कानून के प्रति वफादार रहना चाहिए।
कई नागरिक समाज संगठन इन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। वे ऐसे लोगों के मामले उठाते हैं जिन्हें झूठे प्रकरणों में फंसा दिया गया है परंतु इस तरह के संगठनों की क्षमता सीमित है। ऐसे संगठनों को मज़बूत किया जाना ज़रूरी है। जो लोग झूठे प्रकरणों में लंबी अवधि तक जेलों में पड़े रहते हैं उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए और उन्हें फंसाने वाले पुलिस अधिकारियों को सज़ा दी जानी चाहिए। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को उन लोगों द्वारा लिखी पुस्तकें अनिवार्य रूप से पढ़वाई जानी चाहिए जिन्हें झूठे प्रकरणों में फंसाया गया हो। वे राजनैतिक दल, जो धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के हामी हैं, उन्हें सांप्रदायिक संगठनों को अलग-थलग करने के प्रयास करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सांप्रदायिक दलों के हाथों में सत्ता न आए। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जिसमें न्याय और शांति दोनों हों। किसी धर्म विशेष के व्यक्तियों के साथ इस तरह के घोर अन्याय को कोई समाज और देश स्वीकार नहीं कर सकता। कोई समाज कैसा है, इसका एक मानक यह है कि वह कमज़ोर वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करता है अथवा नहीं। हम केवल यह आशा कर सकते हैं कि जस्टिस काटजू के पत्र को गंभीरता से लिया जाएगा।
(मूल अंग्रेजी से हिन्दी रूपांतरण अमरीश हरदेनिया) (लेखक आई.आई.टी. मुंबई में पढ़ाते थे और सन् 2007 के नेशनल कम्यूनल हार्मोनी एवार्ड से सम्मानित हैं।)